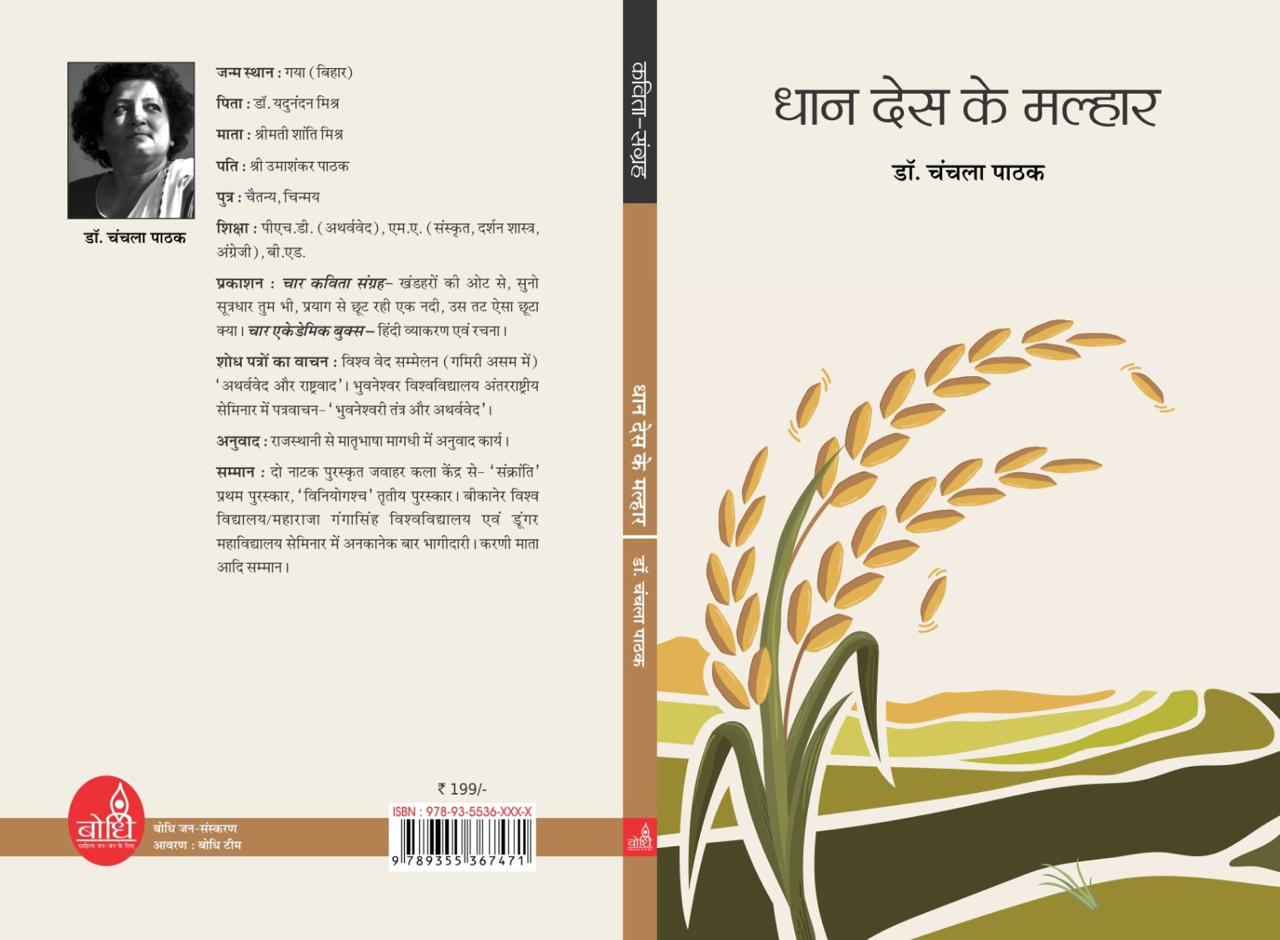
‘धान देस के मल्हार’ शीर्षक सुनते ही लगा मानो धरती माँ अपनी राग में कुहुक उठेंगी। शुरुआती कुछ पन्नों से ही धान की सोंधी ख़ुशबू मेरे साथी बन गए और अंत तक मैं इसकी सुगंध में बिल्कुल वैसे ही डूबता तिरता रहा जैसे एक कविता में चकवी इस सोंधी गंध को हिरण की कस्तूरी-गंध की तरह महसूस करती है।
डॉ चंचला की कविताई बीज के भी मानवीय संवेदन को महसूस करती है।उसकी जागृत अवस्था की ऊष्म-ऊर्जा को “धान के मस्तक पर अँखुआई है एक जिजीविषा, ज्यूँ ज्योतिशिखा” कहते हुए धान की असंख्य मँजरियों की दिव्यता को अपने इन्हीं शब्दों में समेट लेती हैं।
“अँकुर रहा धान, त्याग रहा शनै: शनै:”
जीवन के समूचे दर्शन बोध को समेटे यह पंक्ति शिव के नेत्रमणि की तरह दमकता है। यही तो सृष्टि के सभी चर-अचर की गाथा है। जीवनबोध को यूं आसानी से कह देने का हुनर ही कवि के अंतस के उजास का परिचय भी है।
“अँखुआते होंगे नाभि की गर्माश से… पंकिल जल में बिम्बित हो दहकते होंगे”
यह पंक्ति ऐसी अलौकिक परिकल्पना दर्शाती है मानो कवि इस विषय में आकंठ डूबा हुआ है और धान की ओट में किसी अन्य ईश्वरीय आभा को हमारे प्रत्यक्ष लाने की अप्रतिम कोशिश कर रहा है। कविता अगर अपने अध्यात्म रूप में आ जाए तो कवि ट्रांस को महसूस कर सकता है। इन्हीं ईश्वरीय क्षणों में लिखी जाने वाली कविताओं की छनछनाहट का संगीत हम इन पंक्तियों में सुन सकते हैं। कविता में भात के भाप से उठा सोहर माँ की लोरी के मिठास को बढ़ा रहा है।
“संपुट सुगंध में तर होकर रोमकूपों से फूट पड़ती हैं सहस्र नदियाँ!”
यह कितनी अद्भुत कल्पना है कवि की। यहाँ रूपक व्यंजना से मिलकर कविता को और सुंदर बना रही है। यहाँ कविता का स्वर एक पल के लिए भी अपनी लय और ध्वनि को नहीं छोड़ती। एक ही मूल विषय पर केंद्रित होने के बावजूद पूरे संग्रह में कहीं भी कविताओं का विषयांतर और और भावों का दोहराव नहीं मिलता है।
कवि ने वाक्य की रचना प्रक्रिया पर इस तरह काम किया है कि भावना कल्पना के साथ अनाफोरा (Anaphora) से बाहर निकलती है, जबकि अर्थानुरणन से गूंजती ध्वनियों को साधते हुए कल्पना के साथ बहती है, जिसका एक छोर हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है और यही कविता में असली रस भरता है। धान की ख़ुशबू और फैल जाती है जब कविता में सिनेस्थेसिया का अद्भुत प्रयोग दिखता है, जैसे कवि को इल्हाम हो रहा हो और पंक्तियाँ टपकती जा रही है स्वतः फ़ुहार बनकर। पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे संगीत सुन रहे हों और साथ ही साथ आकार को अपना आकाश ग्रहण करते हुए को देख भी रहे हैं हम।
लिखा है-
“अन्न की अनंत संकल्पनाएँ किसने रची
धान के गाभ में
तुम न जाने कितने कंठों की काकली का
मंत्र-मनन बन विस्तारित हो रही हो बैखरी”
या
“कभी किसी शिशु के माथे को सूंघा है तुमने या कि माँ का थन सद्य तज!”
भाषा का स्वर, आनंद, रस और कवि की मनोदशा सब यह बता रही है कि जिस ईश्वरीय क्षण में कविता रची जाती है उसे कैसे कवि ने साधा है कि धान का रूपक कण-कण में भगवान का प्रमाण दे रहा है। जैसे एक अणु में ब्रह्मांड का दर्शन संभव करा रहा हो कवि।
“उतर तो मैं रही कंठ भर नदी-जल में
और पसर गयी है नदी की पोर-पोर में तुम्हारी देहगंध”
कविता में शब्दों के सुगंध में अनुभूति की रमणीयता अपने लय और ध्वनि को संवार रही है। कवि ने कविता की संरचना में सारे तत्व इस समानुपात में और इस तरह से मिश्रित किए हैं कि पूरा वातावरण बासमती चूड़े की मादक ख़ुशबू में नहा उठा है। खदकते भात का अल्हड़पन और माड़ पर उठती जलतरंग के बीच स्वप्न के ये बीज इसी मादकता को चिह्नित कर रहे हैं।
लिखा है:
“नवोधा पत्नी के कान की लोरियों पर
इन्हीं शब्दों की दहक रखने की शीघ्रता है उसे”
और फिर यह भी कि- “घुटने तक जल में, जल से अधिक पाँक है”। पल भर में ही कितना विस्तार पाती है कविता।
इन कविताओं से गुजरते हुए याद आयी कई कविताएँ मसलन ‘भात’ कविता सुमित त्रिपाठी की, ‘दो वक़्तों का कम से कम तो भात चाहिए’: देवी प्रसाद मिश्र, ‘चप्पल पर भात’-वीरेन डंगवाल, ‘दूध-भात’ प्रतिभा किरण की, ‘भात का भूगोल’-शिरोमणि महतो, बांग्लादेश के कवि ‘रफ़ीक़ आज़ाद’ की मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी ‘भात दे हरामी’ और जोशना बैनर्जी आडवानी की कविता ‘भात’। जबकि इस संग्रह की कविताओं में न ही दोहराव है और न ही याद आयी कविताओं की झलक बस उन कविताओं का भाप है जो स्मृति के झोंके-सी उष्ण गर्माहट देकर ग़ायब हो जाती है।
चंचला लिखती हैं- “ लग्न के धान का विस्तार/ प्रेम से पृथ्वी के पद जाने तक है प्रियंक!”
यहाँ कविताएँ अपने वितान में कई कहानियाँ समाहित किए हुए है। मसलन “हयग्रीव ने किया हयग्रीव का संहार” या बाउल के गीत के द्वारा पत्थरों से फूटते जल के स्रोत की कहानी, पुआल के बिस्तर पर नाचते बचपन का दृश्य, धान के भूसे से दीदिया का रगड़ कर इस बचपन को नहलाना, धान की उपस्थिति के बहाने शादी-विवाह और सोहर जैसे विभिन्न दृश्यों को भी खींच लाना इस बात का भी द्योतक है कि धान हमारे इर्द गिर्द कितनी ख़ुशबू फैलाए है। दुनिया के कई देशों की आबादी भी धान पर ही अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है।
ऐसे कवि का जो लीक से हटकर प्रयोगधार्मिता साधते हुए रचने का अनोखा प्रयास कर रहा हो उसका शत-शत स्वागत है।