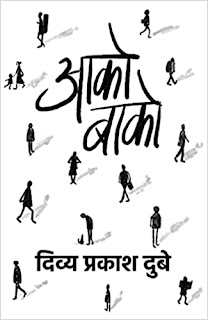
साहित्य जीवन को उसके संवेदनात्मक रूप में दिखाने वाला सशक्त माध्यम होता है। कल्पना या फंतासी बुनते हुए भी कहानीकार हकीकत के आसपास रहता है। जीवनानुभव कहानी को जीवन देते हैं। कई बार यह अहसास होता है कि कहानीकार ने जो लिखा है वह तो हमने खुद देखा या भुगता है। दिव्य प्रकाश दुबे का कहानी संग्रह 'आको बाको' पढ़ते हुए उन्हें बराबर इसका अहसास होता है। इस किताब पर एक समीक्षा यतीश कुमार ने लिखी है। आज पहली बार पर प्रस्तुत है दिव्य प्रकाश दुबे के कहानी संग्रह 'आको बाको' की यतीश कुमार द्वारा की गई समीक्षा 'आस पास के किरदार वाली कहानियाँ'।
जब 'आको बाको' पढ़ना शुरू कर रहा था तो कई पूर्वाग्रहों से घिरा था। यह इसलिए भी क्योंकि दिव्य का लिखा पहली बार पढ़ रहा था। पहली कहानी की शुरुआती रफ्तार से मुझे लगने लगा कि शायद जो मैं सोच के पढ़ रहा हूँ, वही सही है। हालांकि पहली कहानी खत्म होते-होते, खासकर आखिरी के दो पन्नों पर मेरे सारे सवालों का जवाब था। कहानी के किरदार आस-पास से लिए गए हैं। नीता जैसे किरदार शायद हमारे पड़ोस में भी है, हमारी ही नज़र नहीं पड़ती। तब तक जब तक कुछ स्पार्क नहीं हो, जब तक कुछ जोरदार धमाका नहीं हो। दिव्य की कहानियों की एक विशेषता यह है कि हर कहानी में एक संदेश है, कहानियां कुछ कहना चाह रही हैं और शिल्प इतना सहज और सुंदर है कि आप सुनने के लिए बाध्य होते चले जाएंगे।
बतौर पाठक, मेरे लिए ‘आको बाको’ की दूसरी कहानी में ही दिव्य का सम्मोहन बोल रहा था। किताब अब खुल कर बातें कर रही थी। कई बार किरदार के नाम और जगह भी कहानियों से जुड़ने का माध्यम बन जाते हैं। इस कहानी के साथ ऐसा ही हुआ। तरु नामक एक किरदार मेरी एक अधलिखी कहानी का हिस्सा है, तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गयी। मुंबई प्यारा और पसंदीदा शहर है तो थोड़ा और आकर्षित हुआ, आभासी दुनिया से मुझे बेहतरीन दोस्त सापेक्ष मिले, तो पढ़ते हुए यह कहानी मेरे भीतर उतरती चली गई। संयोगवश मेरी कहानियों के किरदार का नाम भी तरु और छाया है, शायद इसलिए भी पढ़ते हुए मुझे अपने किरदार थोड़े से घुले मिले, ऐसा इसलिए भी क्योंकि कहानी जब सर चढ़ती है तो अपनी सी लगने लगती है। है न!
दिव्य के लेखन की एक सुंदर बात यह भी है कि वे छोटी-छोटी पंक्तियों में बड़ी बातें कह देते हैं। कई बार ऐसी पंक्तियां जो पाठक को चकित कर देती हैं। एक जगह कुछ ऐसा ही लिखा है- "बड़े लोगों से भगवान खो जाते हैं, जैसे बच्चों से खिलौना खो जाता है"।
ऐसी पंक्तियां कई जगहों पर हैं। तीसरी कहानी में 15 साल बाद लौटे बाबा से पोता प्रश्न करता है कि - गौतम बुद्ध क्यों नहीं लौटे और बाबा जवाब देते हैं कि "उनको रास्ता याद ही नहीं आया"! और अंत में मारके की बात कि जो गए वो गौतम बुद्ध हुए या नहीं पता नहीं, पर जो लौटे वो गौतम बुद्ध से कम नहीं थे।
दिव्य लिखते हैं- मन के अंधेरे से लड़ना नहीं होता, उसको दुलार से सहलाने पर ही उजाले की किरण दिखनी शुरू होती है। तो इस उजाले-अंधेरे की स्थिति से जो किरदार उभर कर मानस के सितारे बनते हैं वे इन कहानियों को संजीदगी से पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं और दिव्य के किरदार दिव्य के जैसे ही मासूम हैं। संजीव कुमार जैसे दिखने वाले कलाकार एक डाकिए में दिखता है, जिसके डाक ठप्पे में लेखक संगीत सुनता है या वो बूढ़ी दादी जो तरु और पार्थ को एक रात का बसेरा देती है। ये किरदार अपना फैलाव या अपना चँदोवा खुद बुनते हैं।
कहते-कहते दिव्य कुछ अदृश्य सच को भी बहुत आसानी से उकेर देते हैं। मसलन "हर लेखक कभी-न-कभी खाली होता है, मानना नहीं चाहता। खाली होना मौत जितना ही बड़ा सच है।”
'पहला पन्ना' में न जाने कितनी कहानी की परतें हैं और हर परत एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती नज़र आएंगी। कभी ‘कितने पाकिस्तान’ पढ़ी थी, वहां एक अदीब समय से बातें करता है, यहां एक शायर किरदारों से। कुछ कहानियां तो दो पंक्तियों में सिमटी हैं। जैसे 62वें पन्ने के छठे पैराग्राफ में लिखा है- "शायर ने लडक़ी से कागज माँगा, पर लड़की अपना पीठ सामने कर दी। शायर ने पीठ पर अपना एक आँसू रख दिया। लड़की को तुरंत नींद आ गयी। इतनी गहरी नींद में वो आखिरी बार तब सोई थी, जब एक लड़के के साथ भागी थी।‘ आगे लेखक लिखता है- शायर के हाथ को आखिरी बार सब लड़कियाँ ऐसे छू रही थीं, जैसे संगम में नदियाँ एक-दूसरे को छूती हैं। छू कर कुछ देर तक अपने अंदर लहर महसूस करती रहीं। फिर बहुत आगे लिखा है- उन्होंने एक -दूसरे को ऐसे संभाला जैसे टोकरी में सब्जियां एक-दूसरे को संभालती हैं। यह दिव्य के लेखन की ही जादूगरी है कि चंद पंक्तियों में वो एक इंद्रधनुष खींच देते हैं। जिसे पढ़ते हुए कभी लगेगा गुलज़ार का ‘रावी पार’ पढ़ रहे हैं तो कभी सूफी टच के साथ अनामिका की 'आईनासाज़’।
संकलन की 16 कहानियों में भी कहीं कोई दोहराव नहीं है। ये कहानियाँ अलग दिशाओं में खींची त्रिज्यायें हैं जिसे जोड़ने से उस संग्रह का सुंदर वृत आपके सामने है। एक लेखक का रेंज तब समझ में आता है जब उसका शिल्प कथ्य के अनुसार बदलता जाए, शब्दों के अभिव्यक्तियों, व्यंजनाओं में दोहराव न हो। दिव्य इस मामले में खरे उतरते हैं। हर कहानी का कथ्य और शिल्प भिन्न है। दिव्य अपने लेखन में सेट पैटर्न को तोड़ते हैं और आज के लेखकों में ऐसा मिलना सुखद है।
जैसे नव शिशु के पांव की छाप को हम घर में संभाल कर रखते हैं उसी तरह अच्छी कहानियों की छाप कहीं दिल में संभल कर रहती हैं। दिव्य की कहानियों के साथ यही जुड़ाव रहता है। कहानी का एसेंस साथ रह जाता है और यह एक लेखक और उसके किरदारों की जीत है। कहानियां पढ़ते- पढ़ते पाठक खुद कुछ किरदारों को जिंदा करने लगता है। उनकी यात्रा कविता के बाहर भी देखने लगता है जैसे 'पहला पन्ना' में एक शायर मरने से पहले अपनी कविताएं एक औरत को सौंप देता है और 'कविता कहाँ से आती है!' में एक औरत हामिद के पास खान साहब की लिखी कविताएँ उनके मरने के बाद ले कर आती है।
जैसे कविता ज्यों-ज्यों अंत की ओर बढ़ते हुए धारदार होती जाती है, दिव्य की कहानी उसी तर्ज पर, उसी कसक, धसक और ठनक के साथ अंत तक आते-आते मीठी छुरी बन जाती है। वह भी टटका प्रेम वाली कसक लिए।
मैं मानता हूं, कहानी की असल जीत तब है जब पाठक अपनी कहानी उन कहानियों में तलाशने लगे, शब्द उसे निजी लगने लगे। ‘60 सेकंड’ कहानी पढ़ते हुए मुझे मेरा अपना लिखा संस्मरण याद आ रहा था। मौत की दस्तक को लेकर लिखा वह संस्मरण 'पहली बार ब्लॉग' पर प्रकशित है। यहां कहानी में थोड़ा परिवर्तन है, यहां नायक को मौत बुलाती है वहां मेरे पास मौत आती थी।
'गुमशुदा' कहानी पढ़ते हुए भी मैं अचंभित हुआ। मेरी लेखनी में स्वदेश दीपक का बहुत अहम रोल है। विशेषकर गद्य पर कविताई का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 'मैंने मांडू नहीं देखा' से ही हुआ और यहां दिव्य के फंतासी में स्वदेश दीपक को एक किरदार की तरह मिल रहा हूँ। ‘गुमशुदा’ कहानी को मैं इस लिए भी पूरी तरह समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वदेश दीपक का लिखा लगभग पढ़ा है। दिव्य ने अपनी कहानी में जिस औरत का किरदार गढ़ा है वो कोलकाता से स्वदेश के साथ है यह मैं उसी हक़ से कह सकता हूँ। आम पाठक जिन्होंने स्वदेश दीपक को नहीं पढ़ा है उनके लिए इस कहानी में डूबना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा पर कथ्य और फंतासी गढ़ने का शिल्प इतना मासूम है कि आप इसकी गिरफ्त में होंगे। कई कारणों से मैं इस कहानी को दो-तीन दफा पढ़ गया। फिर गहरी सांस ली कि चलो अब एक युवा लेखक मिला जो विनोद कुमार शुक्ल के फंतासी दुनिया की सैर करना जानता है ।
'खुश रहो' कहानी का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। कहानी आधे रास्ते पर जा कर खुलती है और पता चलता है कि कहानी का किरदार में पिता क्या करने जा रहा है और किस चीज के लिए बेटे के पास आये थें। अंत वाली बात बड़ी प्यारी है कि- बहुत कम ऐसा होता है कि बाप को जीते जी माफी मिलती है वरना इतिहास गवाह है, बाप को माफी मरने के बाद ही मिली है। यहां एक बात और दर्ज कर रहा हूँ कि दिव्य के भीतर एक सुखी बच्चा है जिसकी किलकारियां उसे नकारात्मक कहानियों से बचाये रखती हैं और इसलिए यहां हर छोटी से बड़ी कहानियों का अंत सुखद है। यहां इस कहानी में बेटे का बाप को माफ करना भी कहानी का एक सुखद अंत ही है।
दिव्य की एक और खासियत है उसे कहानियों की गति पर नियंत्रण करना आता है। जो कहानी शुरुआत में ढीली लगती है वो भी एक या फिर ज्यादा से ज्यादा दो पन्ने के बाद गज़ब का आकर्षण पैदा कर देती है। अंततः यही कहूँगा, 'आको बाको' का स्वागत किया जाना चाहिए और साल की पहली किताब मेरे लिए पठनीय रही, इसके लिए लेखक का विशेष धन्यवाद।